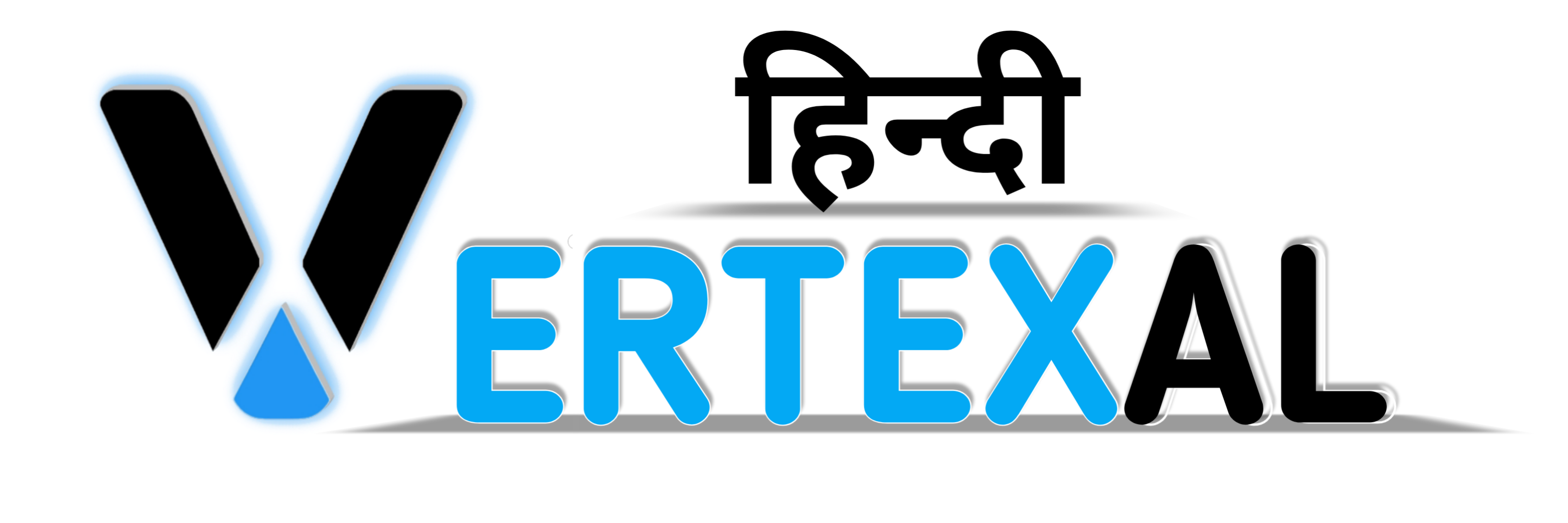कम्प्यूटर के अन्तर्गत मेमोरी का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा Memory के प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
मेमोरी Memory मानव के समान कम्प्यूटर की भी अपनी मेमोरी (memory) होती है, जिसका प्रयोग कम्प्यूटर में डाटा व दिशा-निर्देशों का संग्रह करने तथा जरूरत पड़ने पर उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह कम्प्यूटर का वह भाग है, जिसमें सभी डाटा और प्रोग्राम स्टोर किये जाते हैं। यदि यह भाग न हो तो कम्प्यूटर को दिया जाने वाला कोई भी डाटा तुरन्त नष्ट हो जायेगा। इसलिए इस भाग का महत्त्व स्पष्ट है। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है-प्राइमरी मेमोरी (primary memory) तथा सेकेण्डरी मेमोरी (secondary memory)। इनमें से प्राइमरी मेमोरी को सी०पी०यू० का भाग माना जाता है तथा सेकेण्डरी मेमोरी उससे बाहर चुम्बकीय माध्यमों (magnetic mediums); जैसे- हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्कैट, टेप आदि के रूप में होती है। दोनों प्रकार की मेमोरी में लाखों की संख्या में बाइट (bytes) होती हैं, जिनमें सभी प्रकार का डाटा और आदेश बाइनरी संख्या (binary numbers) के रूप में भण्डारित किये. जाते हैं। किसी कम्प्यूटर की प्राइमरी मेमोरी का आकार जितना ज्यादा होता है, वह उतना ही तेज माना जाता है। कम्प्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है- प्राइमरी मेमोरी तथा सेकेण्डरी मेमोरी। इन दोनों प्रकार की मेमोरियों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है-
प्राइमरी मेमोरी (Primary Memory)
इसे आन्तरिक (internal) या मुख्य (main) मेमोरी या अर्द्धचालक मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह कम्प्यूटर की सी०पी०यू० का ही भाग होती है। इसमें लाखों की संख्या में बाइट (bytes) होती हैं। प्रत्येक बाइट 8 लगातार बिटों (bits) की एक श्रृंखला होती है। बिट सूचना की सबसे छोटी इकाई है। बिट को एक स्विच या बल्ब की तरह समझा जा सकता है। कोई बल्ब या तो जल रहा होता है या बुझा होता है। इन दो स्थितियों को हम क्रमशः ऑन (On) या ऑफ (Off) कहते हैं। इन दो के अलावा कोई तीसरी स्थिति सम्भव नहीं होती। इसी तरह किसी बिट की भी दो स्थितियाँ हो सकती हैं, जिन्हें हम ऑन या ऑफ कहते हैं। सुविधा के लिए हम इन स्थितियों को क्रमशः 1 तथा 0 से व्यक्त करते हैं।
किसी बाइट में से ऐसी ही 8 लगातार बिटें शामिल होती हैं। इन बिटों की स्थितियों के अनुसार बाइट का मान (value) या अर्थ निकाला जाता है। मेमोरी में बाइट को ही सबसे छोटी इकाई माना जाता है। मेमोरी की प्रत्येक बाइट का एक विशेष पता (address) होता है। जिस प्रकार किसी शहर में मकानों पर नम्बर पड़े होते हैं, उसी प्रकार मेमोरी, में बाइटों पर क्रम संख्याएँ पड़ी हुई मानी जाती हैं। ये क्रम संख्याएँ शून्य से प्रारम्भ होती हैं। इन संख्याओं को ही बाइटों का पता कहा जाता है।
कम्प्यूटर की प्राइमरी मेमोरी का आकार गीगाबाइटों में नापा जाता है। साधारण छोटे कम्प्यूटरों की प्राइमरी मेमोरी 1 गीगाबाइट से लेकर 4 गीगाबाइट तक होती है। बड़े कम्प्यूटरों की प्राइमरी मेमोरी कई गीगाबाइटों की भी हो सकती है। प्राइमरी मेमोरी में डाटा तथा उस समय चल रहे प्रोग्राम (या प्रोग्रामों) को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। जैसे ही उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, उन्हें हटाकर दूसरे डाटा या प्रोग्राम उस जगह रखे जा सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी का आकार सीमित होता है, परन्तु इसकी गति बहुत तेज होती है, ताकि जब भी किसी डाटा की जरूरत हो, इसमें से तुरन्त लिया जा सके।
प्राइमरी मेमोरी को भी उसके उपयोग के अनुसार कई भागों में बाँटा जाता है, जो निम्न प्रकार है-
1. रीड़-ओनली मेमोरी Read-Only Memory or ROM
यह प्राइमरी मेमोरी का वह भाग है जिसमें रखी गयी सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है। उस पर न तो कुछ लिखा जा सकता है और न ही उसे बदला जा सकता है। इसमें रखी गयी सूचनाएँ कभी नष्ट नहीं होतीं, क्योंकि बिजली बन्द कर दिये जाने पर भी इसमें लिखी गयी सूचनाएँ बनी रहती हैं। वास्तव में इस भाग में ऐसी सूचनाएँ या प्रोग्राम होते हैं, जो कम्प्यूटर निर्माता द्वारा इसमें भरे जाते हैं और जिनकी आवश्यकता सी०पी०यू० को बार-बार पड़ती है; जैसे-बेसिक इनपुट-आउटपुट सर्विसेज (Basic Input-Output Services) या BIOSI
2. रेण्डम एक्सेस मेमोरी Random Access Memory or RAM
यह मेमोरी का वह भाग है, जिसका उपयोग हम (अर्थात् हमारे प्रोग्राम) अपनी आवश्यकता के अनुसार चाहे जिस तरह कर सकते हैं। हम इसमें रखी गयी सूचनाओं को बार-बार बदल भी सकते हैं। हमारे डाटा और प्रोग्रामों को चलाते समय इसी भाग में रखा जाता है। प्रोग्राम समाप्त हो जाने पर ये सूचनाएँ भी वहीं समाप्त हो जाती हैं। कम्प्यूटर की बिजली बन्द हो जाने पर इस भाग में लिखी गयी सूचनाएँ नष्ट हो जाती हैं।
3. प्रोग्रामेबिल रीड-ओनली मेमोरी Programmable Read-Only Memory or PROM
यह प्राइमरी मेमोरी का वह भाग है, जो रीड ओनली मेमोरी जैसा ही होता है, परन्तु प्रारम्भ में बिल्कुल खाली होता है। उपयोगकर्ता एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा अपनी जरूरत की सूचनाएँ इसमें लिख सकता है, जिन्हें बाद में बदला नहीं जा सकता बल्कि केवल पढ़ा जा सकत है। कम्प्यूटर बन्द कर दिये जाने पर भी ये सूचनाएँ मेमोरी में बनी रहती हैं।
4. इरेजेबिल एण्ड प्रोग्रामेबिल रीड-ओनली मेमोरी Erasable and Programmable Read-Only Memory or EPROM
जैसाकि इनके नाम से स्पष्ट है कि इस भाग में लिखी गयी सूचनाओं को मिटाया भी जा सकता है तथा वहाँ पर नयी सूचनाएँ लिखी जा सकती हैं। इसका शेष उपयोग रीड-ओनली मेमोरी की तरह किया जाता है। इस भाग में लिखी गयी सूचनाओं को मिटाने के लिए इस पर एक विशेष उपकरण से पराबैंगनी किरणें (Ultra-Violet Rays) लगभग 20 मिनट तक डाली जाती हैं।
5. इलेक्ट्रिकली इरेजेबिल एण्ड प्रोग्रामेबिल रीड-ओनली मेमोरी Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory or EEPROM
मुख्य मेमोरी में कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि उसमें लिखी गई सूचनाओं को केवल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों द्वारा मिटाया जा सकता है और उन पर इच्छानुसार सूचनाएँ लिखकर उपयोग किया जा सकता है। सूचनाएँ मिटाने के लिए एक विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है।
सेकेण्डरी मेमोरी Secondary Memory
इस प्रकार की मेमोरी सी०पी०यू० से बाहर होती है, इसीलिए इसे बाह्य (External) या सहायक (Auxiliary) मेमोरी भी कहा जाता है। कम्प्यूटर की प्राइमरी मेमोरी बहुत महँगी होने तथा बिजली चन्द कर देने पर उसमे रखी अधिकतर सूचनाएँ नष्ट हो जाने के कारण न तो हम उसे इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं और न हम उसमें कोई सूचना स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हमे सेकेण्डरी मेमोरी का उपयोग करना पड़ता है। इसकी कीमत तुलनात्मक दृष्टि से वहुत कम और डाटा स्टोर करने की क्षमता (Capacity) बहुत अधिक होती है।
इसमें एक ही कमी है कि इन माध्यमों में डाटा को लिखने (अर्थात् स्टोर करने) तथा पढ़ने (अर्थात् प्राप्त करने) में समय बहुत लगता है। इसलिए हम इसमें ऐसी सूचनाएँ भण्डारित करते हैं जिन्हें लम्बे समय तक सुरक्षित रखना हो तथा जिनकी आवश्यकता लगातार नहीं पड़ती हो।
हम सेकेण्डरी मेमोरी को अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी सीमा तक बढ़ा सकते हैं। यह मेमोरी कुछ चुम्बकीय उपकरणों के रूप में होती है; जैसे- फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, चुम्बकीय टेप, सीडी-रोम (CD-ROM) आदि। सेकेण्डरी मेमोरी का उपयोग बैकअप (Backup) के लिए किया जाता है। जब हमें किसी डाटा की तत्काल आवश्यकता
नहीं रहती, तो उसे किसी चुम्बकीय माध्यम; जैसे- फ्लॉपी डिस्क या चुम्बकीय टेप पर नकल करके अलग सुरक्षित कर
लिया जाता है। ऐसा प्रायः हार्ड डिस्क को खाली करने के लिए किया जाता है, ताकि उस पर ऐसा डाटा भरा जा सके, जिसकी आवश्यकता पड़ रही हो और डिस्क पर जगह न हो। वैकअप साधन में भण्डारित किये गये डाटा को आगे कभी भी आवश्यकता पड़ने पर फिर हार्ड डिस्क पर उतारा या नकल किया जा सकता है। सेकेण्डरी मेमोरी से सम्बन्धित उपकरणों या डिवाइसेज को मास स्टोरेज मीडिया एवं डिवाइसेज भी कहा जाता है।
सेकेण्डरी मेमोरी से सम्बन्धित भण्डारण युक्तियाँ Storage Devices Related to Secondary Memory •
भण्डारण युक्तियाँ; इस प्रकार की युक्तियाँ हैं, जिनका प्रयोग कम्प्यूटर में डाटा-संग्रहण (Data Storage) में किया जाता है, जब बहुत अधिक मात्रा में डाटा संगृहीत करना होता है तो इन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इन पर संगृहीत किया गया डाटा पर्याप्त समय तक बिना क्षतिग्रस्त हुए बना रह सकता है। यहाँ तक कि कम्प्यूटर की विद्युत सप्लाई बन्द होने पर भी इनमें संग्रहीत डाटा को कोई क्षति नहीं पहुँचती। इन युक्तियों में संग्रहीत डाटा को आवश्यकतानुसार पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कुछ प्रचलित भण्डारण युक्तियाँ निम्नलिखित है-
- फ्लॉपी डिस्क,
- हार्ड डिस्क ड्राइव,
- सी०डी० या कॉम्पैक्ट डिस्क,
- मैग्नेटिक या चुम्बकीय टेप,
- डी०वी०डी० या डिजिटल वसेंटाइल डिस्क तथा
- पेन ड्राइव।
1. फ्लॉपी डिस्क Floppy Disk
इसका प्रयोग कम्प्यूटर में कम मात्रा में डाटा संग्रहीत- करने तथा डाटा को पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क को सर्वप्रथमगया था तथा उसे हार्डबोर्ड के कवर में रखा गया था। इसको आसानी से मोड़ा जा सकता था। लोचनीयता (flexibility) के इस गुण के कारण ही इसका नाम फ्लॉपी पड़ा। यह फ्लॉपी केवल 1 मेगाबाइट डाटा ही संग्रहीत कर सकती थी। बाद में 5.25 इंच आकार वाली (डायमीटर में), 3.5 इंच आकार वाली (डायमीटर में) फ्लॉपियाँ प्रस्तुत की गईं। फ्लॉपी डिस्क में डाटा संग्रह करने वाला माध्यम Mylar या Vinyl Plastic का बना। यह आकार में गोल होता हैं जिसकी एक या दोनों सतहों पर चुम्बकीय पदार्थ (Iron oxide) का लेप होता है जिसके कारण उस सतह पर डाटा संग्रहीत किया जा सकता है। यदि चुम्बकीय पदार्थ का लेप एक तरफ होता है तो इसे Single Sided Floppy तथा यदि दोनों तरफ लेप होता है तो इसे Double Sided Floppy कहते हैं। धूल तथा गर्मी से बचाने के लिए ही इस माध्यम को प्लास्टिक के कवर (Jacket) में रखा जाता है।
प्रत्येक फ्लॉपी की सतह पर संकेन्द्रिय गोलाकार छल्लों के रूप में ‘ट्रैक’ होते हैं। इनकी संख्या अलग-अलग प्रकार की फ्लॉपी में अलग-अलग होती है। मिनी फ्लॉपी (Mini Floppy) में ट्रैक की संख्या 35 से 40 तथा माइक्रो फ्लॉपी (Micro Floppy) में 40 से 80 तक होती है। ये ट्रैक छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त होते हैं, जिन्हें ‘सेक्टर’ कहा जाता है।
फ्लॉपी को इनके आकार तथा संग्रह-क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। आकार के आधार पर फ्लॉपी को * मिनी फ्लॉपी तथा माइक्रो फ्लॉपी में विभक्त किया गया है तथा संग्रह क्षमता के आधार पर इन्हें Single Density, Double Density तथा High Density में विभक्त किया गया है। इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित ट्रैक की संख्या को कहते हैं।
डाटा की संग्रह क्षमता के आधार पर फ्लॉपियों को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है-
- (i) Single Sided – Single Density
- (ii) Single Sided – Double Density
- (iii) Single Sided – High Density
- (iv) Double Sided – Single Density
- (v) Double Sided – Double Density
- (vi) Double Sided – High Density
फ्लॉपी एक आसानी से उपलब्ध होने वाली, वजन में हल्की, कीमत में सस्ती भण्डारण युक्ति है। इसका विशेष गुण यह है कि यह एक पोर्टेबल (Portable) भण्डारण युक्ति है अर्थात् इसमें डाटा संग्रहीत करके आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जा सकता है। परन्तु इसकी डाटा संग्रहण क्षमता कम होती है तथा बार-बार प्रयोग करने से ये जल्दी ही
खराब हो जाती है। धूल, धूप तथा नमी के सम्पर्क में आकर भी ये खराब हो जाती है। वर्तमान समय में फ्लॉपी डिस्क का स्थान सी०डी० एवं डी०वी०डी० ने ले लिया है।
फ्लॉपी ड्राइव Floppy Drive
फ्लॉपी पर डाटा को लिखने तथा पढ़ने के लिए हमें फ्लॉपी ड्राइव (floppy drive) की आवश्यकता होती है। फ्लॉपी ड्राइव में एक लोहे के बॉक्स (box) के अन्दर रीड/राइट हैड (Read/Write Head) लगा रहता है, जिसके द्वारा डाटा लिखा व पढ़ा जाता है। इनमें लगी मोटरों में से एक मोटर फ्लॉपी के मीडिया (डिस्क) को घुमाने तथा दूसरी रीड/राइट हैड (Read/Write Head) को आगे-पीछे चलाने के काम आती है।
फ्लॉपी ड्राइव से डाटा चुम्बकीय व गैर-चुम्बकीय स्पॉट (spots) के रूप में लिखा जाता है, जिनमें से चुम्बकीय स्पॉट (spot) 1 को तथा गैर-चुम्बकीय स्पॉट (spot) 0 को प्रदर्शित करता है।
2. हार्ड डिस्क ड्राइव Hard Disk Drive
फ्लॉपी की भांति ही हार्ड डिस्क भी डाटा-संग्रह के काम आती है, परन्तु फ्लॉपी की तुलना में, हार्ड डिस्क अधिक मात्रा में डाटा संग्रहीत कर सकती है। आजकल पर्सनल कम्प्यूटर में 500 GB तक की हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जा रहा है। इससे अधिक क्षमता की हार्ड डिस्क भी बाजार में उपलब्ध है। हार्ड डिस्क की डाटा स्थानान्तरण की गति भी फ्लॉपी से बहुत अधिक होती है। बार-बार नया डाटा लिखने व मिटाने से फ्लॉपी डिस्क की भाँति ये खराब नहीं होती है। हार्ड डिस्क को कम्प्यूटर में स्थायी रूप से लगाया जाता है जिससे इसे बार-बार नहीं निकालना पड़ता और यह धूल तथा नमी से बची रहती है।
हार्ड डिस्क में डाटा संग्रह करने वाला माध्यम (Mylar या Vinyl Plastic के स्थान पर) धातु का बना होता है। इसीलिए इसे हार्ड डिस्क कहते हैं। ड्राइव (drive) शब्द लोहे के बॉक्स के लिए प्रयुक्त होता है, जिसमे रीड/राइट हैड (Read/Write Head) लगे रहते हैं। इसमें हम Disk लगाकर डाटा को पढ़ते व लिखते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव में एक ही लोहे के बॉक्स के अन्दर, डिस्क तथा रोड/राइट हैड (Read-Write Head) स्थायी रूप से लगे रहते हैं, इसलिए इसे हार्ड डिस्क ड्राइव (Hard Disk Drive) कहा जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव के अन्दर घातु की बनी दो या दो से अधिक गोलाकार डिस्क होती हैं, जिन्हें प्लेटर (platter) कहते हैं। इनकी दोनों सतहों पर चुम्बकीय पदार्थ का लेप होता है। इन प्लेटर्स (platters) पर भी पलॉपी की भांति ही संकेन्द्रीय गोलाकार छल्ले होते हैं, जिन्हें ‘ट्रैक’ कहते हैं। ये ट्रैक छोटे-छोटे भागो में विभक्त होते हैं, जिन्हें ‘सेक्टर’ कहते हैं। इन्हीं सेक्टरों पर डाटा लिखा जाता है।
हार्ड डिस्क ड्राइव में लगे प्लेटर्स (platters) में सबसे ऊपर लगे प्लेटर (platter) की ऊपरी सतह तथा सबसे नीचे लगे Platter की निचली सतह पर डाटा नहीं लिखा जाता है अर्थात् हार्ड डिस्क ड्राइव की Recording surface इसमें लगे कुल प्लेटर्स (platters) की संख्या के दोगुने से दो कम होती है।
(Recording Surface Total No. of Platters x 2-2)
हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार Types of Hard Disk Drive – हार्ड डिस्क ड्राइव में लगे हैड को निम्न दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है-
- (i ) स्थायी हैड Fixed Head स्थायी हैड (fixed head) वाली हार्ड डिस्क ड्राइव में हैड (head) आगे-पीछे गति नहीं करते हैं तथा इसमें एक सतह पर डाटा लिखने व पढ़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले हैड (head) की संख्या, उस
सतह पर उपस्थित ट्रैक (Track) की संख्या के बराबर होती है। स्थायी हैड (fixed head) वाली हार्ड डिस्क ड्राइव गति में, गतिशील हैड ( movable head) वाली हार्ड डिस्क ड्राइव से तेज होती है। - (ii) गतिशील हैड Movable Head गतिशील हैड (Movable Head) वाली हार्ड डिस्क ड्राइव में हैड (Head) आगे-पीछे गति कर सकते हैं तथा इसमें सतह पर डाटा लिखने-पढ़ने के लिए केवल एक ही हैड (Head) प्रयुक्त किया जाता है। यह हैड (Head) आगे-पीछे गति करके सभी ट्रैक्स (Tracks) के सेक्टर (Sector) पर जाकर डाटा लिखता-पढ़ता है।
जब हार्ड डिस्क ड्राइव में डाटा को लिखा व पढ़ा नहीं जा रहा होता है, तब रीड/राइट हैड (Read/Write Head) प्लेटर (Platter) के ऊपर टिके रहते हैं, परन्तु जब हार्ड डिस्क ड्राइव में डाटा को लिखा व पढ़ा जाता है, तब प्लेटर (Platter) गोल-गोल घूमने लगते हैं। इनके घूमने के कारण उत्पन्न हुए वायु-दाब से इन प्लेटर्स (Platters) के ऊपर टिके हैड 1 इंच के 400 वें भाग के बराबर ऊपर जाकर, डाटा को पढ़ने व लिखने लगते हैं। इसमें प्लेटर की सतह को कोई नुकसान नहीं होता।
3. सी०डी० या कॉम्पैक्ट डिस्क CD or Compact Disc
आजकल सी०डी० का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। यह संरचना में गोल डिस्कनुमा होती है। इस पर लेजर किरणों के द्वारा डाटा को लिखा जाता है। सी० डी० को सर्वप्रथम Philips और Sony ने प्रस्तुत किया था। इसमें एक पतले आकार (120 मिमी) की गोल व सिल्वर तथा ऐलुमिनियम की पर्त होती है, जिस पर Poly Carbonate Plastic की पतली पर्त होती है। सी०डी० निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है-
- (i) सी०डी०-रोम CD-ROM इसको सी०डी०-रोम इसलिए कहा जाता है, क्योकि इस प्रकार की सी० डी० को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, अर्थात् इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- (ii) सी०डी०-आर० CD-R सी०डी० आर में डाटा एक बार लिखा जा सकता है। इसके उपरान्त इसको केवल पढ़ा जाता है। सी०डी०-आर में डाटा लिखने को बर्न कन्टेन्ट से भी सम्बोधित करते हैं। विशिष्ट मल्टीसेशन बर्न स्थिति में डाटा को एक से अधिक बार सी०डी०-आर में लिखा जा सकता है। इसमें डाटा लिखने के लिए एक विशेष युक्ति सी०डी० राइटर (CD-Writer) का प्रयोग किया जाता है।
- (iii) सी०डी०-आर डब्ल्यू CD-RW इसमें डाटा को पढ़ने के अलावा अनेक बार लिखने की भी सुविधा होती है। डाटा लिखने के लिए इसमें भी सी०डी० राइटर (CD-Writer) का प्रयोग किया जाता है। सी०डी० (CD) में फ्लॉपी व हार्ड डिस्क के विपरीत, ट्रैक न होकर, घड़ी की स्प्रिंग की तरह का एक Spiral आकार का ट्रैक होता है। यह ट्रैक छोटे-छोटे सेक्टर्स (Sectors) में विभक्त होते हैं। सी०डी० (CD) बदलती हुई गति से घूर्णन करती है। डिस्क की निरन्तर बदलती हुई गति इस प्रकार समायोजित की जाती है कि यह एक स्थिर रैखिक वेग (Constant Linear Velocity) से गुजरे।
सी०डी० ड्राइव C.D. Drive
सी०डी० ड्राइव के द्वारा सी०डी० से डाटा पढ़ा व लिखा जाता है। सी०डी० ड्राइव एक लोहे के बॉक्स के रूप में होती है जिसमें सी०डी० को पढ़ने या लिखने के लिए प्रविष्ट किया जाता है। सी०डी०-आर में डाटा लिखने के लिए जले क्षेत्रों (Burned Areas) और बिना जले क्षेत्रों (Unburned Areas) का प्रयोग किया जाता है। इसमें बिना जला क्षेत्र 1 को व जला क्षेत्र 0 को प्रदर्शित करता है। सी०डी० में जहाँ-जहाँ भी शून्य लिखना होता है वहाँ लेजर बीम की एक तीव्र किरण को डालकर इसकी सतह के रंग को जलाकर एक छोटा काला धब्बा बना दिया जाता है। इसे जला क्षेत्र कहते हैं। जहाँ-जहाँ पर सी०डी०-आर पर 1 लिखना होता है, वहाँ-वहाँ पर लेजर
उत्सर्जित करने वाली युक्ति के द्वारा कुछ नहीं किया जाता। अतः बिना जली सतह को 1 के रूप में माना जाता है। लेजर
उत्सर्जित करने वाली युक्ति के समीप ही एक प्रकाश संवेदक लगा रहता है, जिसका कार्य सी० डी० से टकराकर लौटने
वाले प्रकाश को विद्युत के रूप में बदलना होता है। जब सी० डी० से डाटा पढ़ा (read) जा रहा होता है तो सी० डी० एक मोटर द्वारा गोल-गोल घूमने लगती है। इसके पश्चात् लेजर उत्सर्जित करने वाली युक्ति के द्वारा इस पर लेजर डाली जाती है। यदि लेजर उत्सर्जित करने वाली युक्ति के सामने बिना जला क्षेत्र (Unburned Area) होता है तो यह लेजर को परावर्तित (change) कर देता है। प्रकाश संवेदक द्वारा यह परावर्तित प्रकाश ग्रहण कर लिया जाता है। इससे उत्पन्न विद्युत को सी०पी०यू० को भेज दिया जाता है, जिसको कम्प्यूटर एक के रूप में मानता है।
इसके विपरीत, जब लेजर उत्सर्जित करने वाली युक्ति के सामने जला क्षेत्र (Burned Area) होता है तो वह आने वाली लेजर को विपरीत दिशा में परावर्तित नहीं करता है, जिस कारण संवेदक पर लेजर का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है तथा यह विद्युत उत्पन्न नहीं करता है। इस स्थिति में कम्प्यूटर इसको शून्य 0 मानता है। इस प्रकार कम्प्यूटर को एक (1) व शून्य (0) के रूप में डाटा प्राप्त होता है। सी० डी० के अन्य प्रकार भी सी०डी०-आर से मिलते-जुलते सिद्धान्त पर कार्य करते हैं।